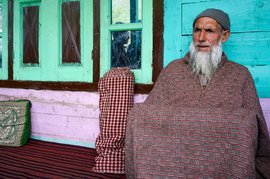“हर बार जब भट्टी जलती है, मैं ख़ुद को जला लेती हूं!”
सलमा लोहार के दोनों टखनों में जलने के बेशुमार दाग़ दिखते हैं और उनके बाएं हाथ की दो ऊंगलियों पर कटने के ताज़ा निशान हैं. वह भट्टी के नीचे से मुट्ठी भर राख निकाल कर घावों पर रगड़ लेती हैं, ताकि वे तेज़ी से भर जाएं,
सलमा (41) का परिवार सोनीपत के बहालगढ़ बाज़ार में उन झुग्गियों में बसे छह लोहार परिवारों में एक है, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं. उन झुग्गियों की तरफ़ भीड़भाड़ वाला बाज़ार है और दूसरी तरफ़ नगरपालिका द्वारा इकठ्ठा किए गए कूड़े का ढेर है. पास ही सरकार का बनाया हुआ एक शौचालय और पानी की टंकी है. सलमा का परिवार पूरी तरह से बस इतनी सी सुविधाओं पर निर्भर है.
इन झुग्गियों में बिजली नहीं है और अगर 4-6 घंटे तक लगातार बारिश होती रहे, तो इनमें पानी का जमाव हो जाता है. पिछले अक्टूबर (2023) में ऐसा ही हुआ था. यह नौबत आने पर उन्हें पानी के कम होने तक अपने पांवों को समेट कर चारपाइयों पर चुपचाप बैठे रहना पड़ता है. इसमें तक़रीबन 2-3 दिन लग जाते हैं. “उन दिनों हमें भयानक दुर्गन्ध का सामना करना पड़ता है,” सलमा का बेटा दिलशाद बताता है.
“लेकिन हम कहीं और जा भी कहां सकते हैं? ” सलमा पूछतीं हैं. “हम जानते हैं कि यहां गंदगी के अंबार के बगल में रह कर हम बीमार पड़ते रहते हैं. यहां बैठने वाली मक्खियां हमारे खाने पर भी आ बैठती हैं. लेकिन हम और कहां जाएं?”
गडिआ, गडिया या गडुलिया लोहार को राजस्थान में ख़ानाबदोश जनजाति (एनटी) के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है. इस समुदाय के लोग दिल्ली और हरियाणा में भी रहते हैं. लेकिन एक तरफ़ जहां दिल्ली में उन्हें ख़ानाबदोश जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, वहीं हरियाणा में वे पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध हैं.
बाज़ार के जिस इलाक़े में वे रहते हैं वह स्टेट हाईवे -11के बगल में बसा है और वहां बड़ी संख्या में ताज़ा साग-सब्ज़ी, मिठाई, किराना, बिजली के उपकरण और दूसरी चीज़ों के खुदरा बिक्रेताओं की दुकानें हैं. स्टालनुमा दुकानों के मालिक बाज़ार बंद हो जाने के बाद चले जाते हैं.


बाएं: सोनीपत के बहालगढ़ बाज़ार में रहने वाले ये लोहार इन झुग्गियों को ही अपना घर कहते हैं. दाएं: सलमा लोहार अपनी नौ साल की भतीजी चिड़िया के साथ हैं


वे लोहे के सामान जैसे रसोईघर और खेती-बाड़ी के उपकरण जैसे चलनी, हथौड़े, कुदाल, कुल्हाड़ी, छेनी, कड़ाही, गंडासा और कई दूसरी चीज़ें बेचते हैं. उनके घर और काम करने की जगहें बाज़ार की सड़क के ठीक किनारे हैं
लेकिन सलमा जैसे लोगों के लिए, यह बाज़ार उनका घर भी है और रोज़गार की जगह भी.
“मेरे दिन की शुरुआत सुबह-सबेरे 6 बजे सूरज के निकलने के साथ ही हो जाती है, क्योंकि मुझे अपनी भट्ठी सुलगानी होती है, अपने परिवार के लिए खाना पकाना होता है, और तब काम पर जाना होता है,” सलमा (41) की कहती हैं. अपने पति विजय के साथ दिन में दो बार उनको लंबे समय तक भट्टी पर काम करना होता है. दोनों लोहे के कबाड़ों को गलाने और पीटने के बाद उनसे नए सामान बनाते हैं. दिन भर में वे चार-पांच सामान बना लेते हैं.
सलमा को अपने कामों से थोड़ी फ़ुर्सत दोपहर के वक़्त मिलती है. इस समय वह अपनी चारपाई पर बैठीं एक कप गरमागरम चाय का स्वाद ले रही हैं और उनके दो बच्चे उनके साथ ही बैठे हैं – उनकी इकलौती बेटी तनु 16 साल की है और सबसे छोटा बेटा 14 साल का है. उनकी देवरानी की बेटियां – शिवानी, काजल और चिड़िया – भी उनके पास ही बैठी हुई हैं. केवल नौ साल की चिड़िया ही स्कूल जाती है.
“क्या आप इसे व्हाट्सऐप कर सकते हैं?” सलमा पूछती हैं, “सबसे पहले मेरे काम के बारे में लिखियेगा!”
उनके व्यवसाय में काम आने वाले औज़ार और तैयार सामान दोपहर की तेज़ धूप में चमक रहे हैं – चलनी, हथौड़े, फावड़े, कुल्हाड़ियां, छेनिया, कड़ाहियां, गंडासे और कई दूसरे तैयार सामन.
“इस झुग्गी में हमारी सबसे क़ीमती चीज़ें हमारे औज़ार हैं,” वह कहती हैं. वह धातु के एक बड़े बर्तन के सामने बैठी हैं. उनका मध्यावकाश समाप्त हो चुका है, और उनके हाथ में चाय की खाली कप की जगह एक छेनी और हथौड़ी आ चुकी है. बहुत आराम से वह बर्तन के पेंदे में हथौड़ी की मदद से छेद बनाती हैं. उनके काम में यह सहजता अभ्यास के कारण आई है. हर दो बार हथौड़ी चलाने के बाद वह छेनी का कोण बदल देती हैं. “यह चलनी रसोईघर के लिए नहीं है. इसका इस्तेमाल किसान अनाज चालने में करते हैं.”


बाएं: सलमा के लिए दिन की शुरुआत सूरज निकलने के साथ होती है. जागने के बाद वह अपने परिवार के लिए खाना पकाती हैं और काम शुरू करने के लिए भट्टी सुलगाती हैं. दोपहर में अपने काम से थोड़ा वक़्त निकालकर वह चाय पीती हैं. दाएं: सलमा ने अपने हाथ में एक पारंपरिक कढ़ाई (मोटी चूड़ी) पहनी हुई है, और उनका बेटा दिलशाद परिवार द्वारा बनाए गए हथौड़े और फावड़े दिखा रहा है


सलमा एक छेनी और हथौड़ी की मदद से चलनी बना रही हैं, जिसका इस्तेमाल किसान अनाज चालने के लिए करेंगे. अभ्यास से हासिल की गई सहजता के साथ हर दो बार हथौड़ी से पीटने के बाद वह छेनी का कोण बदल देती हैं
भीतर, विजय भट्ठी पर काम कर रहे हैं, जिसे उन्हें दिन में दो बार जलाना पड़ता है – एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को. जिस लोहे की सलाख़ को वह आकार दे रहे हैं, वह तपकर लाल हो चुका है, लेकिन उनको धातु के इस ताप की जैसे कोई चिंता ही नहीं है. जब उनसे यह पूछा जाता है कि भट्ठी को सुलगने में कितना समय लगता है, तब जवाब में वह हंस पड़ते हैं, “जब अंदर एक चमक उठेगी, तो हमें पता चल जाएगा. हवा में नमी होने से भट्टी को सुलगने में अधिक समय लगता है. सामान्य रूप से हमें इस काम में एक से दो घंटे लगते हैं, लेकिन यह बहुत कुछ हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले पर निर्भर करता है.”
कोयले की क़ीमत 15 से 70 रुपए प्रति किलो के बीच कुछ भी हो सकती है. यह कोयले की क़िस्म पर निर्भर है. इन्हें थोक मात्रा में ख़रीदने के लिए सलमा और विजय उत्तर प्रदेश के ईंट-भट्ठों तक की यात्रा करते हैं.
विजय निहाई पर लोहे की दहकती सलाख़ को रखकर हथौड़े की मार से उसके सिरे को चिपटा करने का काम शुरू करते हैं. छोटी भट्टी लोहे को पूरी तरह से गला पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ रही है.
लोहार ख़ुद को सोलहवीं सदी के राजस्थान के उस समुदाय का वंशज बताते हैं जिनका पेशा हथियार बनाना था. बाद के सालों में चित्तौड़गढ़ पर मुग़लों के क़ब्ज़े के बाद वे उत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में चले गए. “वे हमारे पूर्वज थे. अब हम बिल्कुल अलग जीवन जी रहे हैं,” विजय मुस्कुराते हुए कहते हैं. “लेकिन आज भी उसी कारीगरी के कामों को कर रहे हैं जो वे हमें सिखा गए. हमने यह जो कढ़ाई [मोटे कंगन] पहनी हुई है, यह भी उनकी ही देन है.”
अब वह इस हुनर को अपने बच्चों को सिखाने में लगे हैं. “इस काम में सबसे होशियार दिलशाद है,” वह बताते हैं. दिलशाद सलमा और विजय की सबसे छोटी संतान है. उपकरणों की तरफ़ इशारा करता हुआ वह कहता है, “ये हथौड़ा हैं. बड़े वाले को घन कहते हैं. बापू गर्म धातु को चिमटे से पकड़ते हैं और उनके उभारों को ठीक-ठीक आकार देने के लिए कैंची का उपयोग करते हैं.”
चिड़िया हाथों से चलाए जाने वाले पंखे की हैंडल को घुमा रही है, जिसे भट्ठी का तापमान नियंत्रित रखा जा सकता है. आसपास सूखी हुई राख उड़ती है, तो वह खिलखिलाती है.


भट्टी की लपटों का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन परिवार को इसी पर निर्भर रहना है


परिवार की दुकान पर सामने रखी चलनियां, खुरपियां और दरांतियां. परिवार के लोग रिंच, हुक, कुल्हाड़ी, गंड़ासा और चिमटा भी बनाते हैं
दुकान पर एक महिला चाक़ू ख़रीदने के इरादे से आती है. सलमा उसे चाक़ू की क़ीमत 100 रुपया बताती हैं. महिला जवाब देती है, “इसके मैं 100 रुपए नहीं दूंगी. मैं प्लास्टिक का बना चाक़ू ख़रीद लूंगी, जो मुझे बहुत सस्ते में मिल जाएगा.” दोनों थोड़ी देर तक मोलभाव करते हैं और आख़िरकार सौदा 50 रुपए में पट जाता है.
महिला के जाने के बाद सलमा एक लंबी सांस लेती हैं. परिवार अपने भरण-पोषण लायक पर्याप्त सामान नहीं बेच पा रहा है. प्लास्टिक के बने सामान उनके बनाए उपकरणों को भारी टक्कर दे रहे हैं. न तो वे अपने उत्पादन को तेज़ी से बढ़ा पा रहे हैं और न क़ीमत के मामले में प्लास्टिक के सामानों का मुक़ाबला कर पा रहे हैं.
“हमने भी अब प्लास्टिक की चीज़ें बेचनी शुरू कर दी है,” वह कहती हैं. “मेरे देवर की अपनी झुग्गी के आगे प्लास्टिक के सामान की एक दुकान है और मेरा भाई दिल्ली के पास टिकरी बॉर्डर पर प्लास्टिक के सामान बेचता है.” वे बाज़ार के दूसरे विक्रेताओं से प्लास्टिक ख़रीदते हैं और दूसरी जगहों पर उन्हें बेचते हैं, लेकिन उन्हें नाममात्र का मुनाफ़ा होता है.
तनु बताती है कि दिल्ली में उसके मामा लोग ज़्यादा कमाई करते हैं. “बड़े शहरों में लोग ऐसी चीज़ों पर अधिक पैसे ख़र्च करते हैं. उनके लिए 10 रुपए का वह महत्व नहीं है. किसी ग्रामीण के लिए यह बड़ी रक़म है और वे इसे हम पर नहीं लुटाना चाहते हैं. यही कारण है कि मेरे मामा अधिक पैसे वाले लोग हैं.”
*****
“मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं,” सलमा कहती हैं. पहली बार मैं उनसे 2023 में मिली थी. मैं पास के एक विश्वविद्यालय में एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी. “मैं चाहती हूं कि वे अपने जीवन में कुछ बनें.” वह इसकी ज़रूरत तबसे अधिक महसूस करने लगी हैं, जबसे उनके बड़े बेटे को ज़रूरी काग़ज़ातों की कमी के कारण सेकेंडरी स्कूल से निकाल दिया गया. अब वह 20 साल का है.
“मैं सरपंच से लेकर ज़िला मुख्यालय तक सभी जगहों के चक्कर काटे. उन्हें आधार, राशनकार्ड जाति से संबंधित वे सभी पेपर दिए जो-जो उन्होंने मांगे. अनगिनत काग़ज़ों पर अपने अंगूठे के निशान लगाए, लेकिन बदले में कुछ भी नही मिला.”


बाएं: विजय बताते हैं कि उनके सभी बच्चों में दिलशाद इस काम में सबसे ज़्यादा माहिर है. दाएं: लोहे को कैंची की मदद से काटना पड़ता है और सही आकार देने के लिए उन्हें चिपटा करना पड़ता है. चूंकि भट्ठी छोटी है और लोहे को गला पाने में असमर्थ है, इसलिए इस काम में बहुत मेहनत लगती है
पिछले साल दिलशाद को भी कक्षा 6 की अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देनी पड़ी. वह कहते हैं, “सरकारी स्कूलों में किसी काम लायक पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मेरी बहन तनु बहुत कुछ जानती है. वह एक पढ़ी-लिखी लड़की है. ” तनु ने आठवीं तक की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन अब वह आगे नहीं पढ़ना चाहती है. पास के स्कूल में 10 तक की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए उसे एक घंटे पैदल चलकर तीन किलोमीटर दूर खेवारा में बने स्कूल में जाना होगा.
“लोग मुझे घूरकर देखते है,” तनु कहती है. “वे गंदे जुमले भी कहते हैं. मैं बता भी नहीं सकती हूं.” इसलिए अब तनु घर पर ही रहती है और काम में अपने मां-पिता का हाथ बंटाती है.
परिवार के सभी लोग सरकारी टैंकर के पास खुले में ही नहाने को मजबूर हैं. तनु धीमी आवाज़ में कहती है, “हमें खुले में नहाते हुए हर कोई देख सकता है.” सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें हर बार 10 रुपए चुकाने पड़ते हैं. पूरे परिवार के लिए यह काफ़ी महंगा पड़ता है. उनकी आमदनी इतनी अधिक नहीं कि वे कोई ढंग का घर किराये पर ले सकें, जिसमें एक शौचालय भी हो. इसलिए मजबूरन उन्हें सड़क पर अपना गुज़ारा करना पड़ता है.
परिवार में किसी को कोविड-19 का टीका नहीं लगा है. बीमार पड़ने की स्थिति में उन्हें बढ़ खलसा या सेवली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) जाना पड़ता है. निजी क्लिनिक महंगे होने के कारण उनके लिए अंतिम शरण स्थल हैं.
सलमा बहुत सोच-समझ कर ख़र्च करती हैं. “जब हाथ तंग हो, तो हम कचरा बीननेवालों से कपड़े ख़रीदते हैं. वहां हमें 200 रुपए में पहनने लायक कपड़े मिल जाते हैं.” वह बताती हैं.
कभी-कभी उनका परिवार सोनीपत के दूसरे बाज़ारों में भी जाता है. तनु बताती है, “हम सब रामलीला देखने जाने वाले हैं, जो पास में ही रामनवमी के मौक़े पर होने वाला है. अगर हमारे पास पैसे रहेंगे, तो हम चाट-पकौड़े भी खाएंगे.”
“भले मेरा नाम मुसलमानों के जैसा है, लेकिन मैं एक हिन्दू हूं ,” सलमा कहती हैं. “हम सबकी पूजा करते हैं – हनुमान, शिव गणेश, सभी ईश्वर की.”
“और अपने काम के माध्यम से हम अपने पुरखों की भी पूजा करते हैं!” दिलशाद अपनी तरफ़ से तुरत जोड़ते हैं. उनकी मां यह सुनकर हंस पड़ती हैं.
*****


बाएं: चूंकि लोहे के सामानों की बिक्री में दिन-बदिन गिरावट होती जा रही है, इसलिए उनके परिवार ने प्लास्टिक के सामान बेचने शुरू कर दिए हैं. दाएं: उन्हें अपनी झुग्गी में अपने साथ एक बछड़े को भी रखना पड़ता है, जिसे उन्हें पास के गांव के किसी आदमी ने दिया है
जब बाज़ार में बिक्री में गिरावट आती है, तो अपना सामान बेचने के लिए विजय और सलमा को आसपास के गांवों में जाना पड़ता है. ऐसा उन्हें महीने में एक या दो बार करना पड़ता है. हालांकि, वे कभीकभार ही गांव जाते हैं, लेकिन जब कभी वे जाते हैं, तो उनकी कमाई बमुश्किल 400-500 रुपए ही होती है. सलमा कहती हैं, “कई बार तो हम इतना पैदल चलते हैं कि लगता है जैसे हमारे पांवों की हड्डियां टूट गई हैं.”
कभी-कभी गांव के लोग उन्हें मवेशी दे देते हैं – छोटे बछड़े जिन्हें अपनी मां का दूध छुड़ाकर उससे अलग कर दिया जाता है. परिवार की कमाई इतनी नहीं है कि वह अपने लिए कोई ढंग का घर किराये पर ले सकें. मजबूरन उन्हें सड़क पर अपना जीवन गुज़ारना पड़ता है.
युवा तनु को उन शराबियों की अनदेखी करनी पड़ती है जो रात के अंधेरे में उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं. दिलशाद कहता है, “हमें कई बार उन्हें पीटना या उन पर चिल्लाना पड़ता है. हमारी मांएं-बहनें यहीं सोती हैं.”
हाल-फ़िलहाल ही कुछ लोगों ने उन्हें यह जगह ख़ाली करने का आदेश दिया है. उन्होंने ख़ुद को नगर निगम (सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) से बताया था. लोहारों से कहा गया है कि झुग्गी के पिछले हिस्से में कचरा फेंकने वाले मैदान में जाने के लिए गेट बनाया जाना है, इसलिए उन्हें अपने क़ब्ज़े की सरकारी ज़मीन खाली करनी पड़ेगी.
वहां आने वाले अधिकारियों ने आधार कार्ड, राशनकार्ड और अन्य काग़ज़ातों के माध्यम से परिवारों के आंकड़े इकट्ठे किए हैं, लेकिन वहां अपने दौरे का कोई अधिकारिक प्रमाण नहीं छोड़ा है. इसलिए यहां रहने वाला कोई आदमी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि वे कौन लोग थे. इस तरह के दौरे हर दो महीने के बाद लगते हैं.
“उन्होंने हमसे वादा किया है कि वे हमें ज़मीन का एक टुकड़ा देंगे,” तनु पूछती है, “कौन सी ज़मीन ? कहां? क्या वह बाज़ार से दूर है? उन्होंने हमें यह सब नहीं बताया है.”


नौ साल की चिड़िया बुझी हुई भट्टी से राख को हटाने के लिए एक हाथ से संचालित पंखे का उपयोग करती है. परिवार की कमाई विगत सालो में घटकर बहुत कम रह गई है. हालांकि वे व्यस्त बाज़ार के बीचोबीच काम करते हैं, फिर भी महामारी के बाद उनकी बिक्री में ख़ासी कमी आई है
परिवार का आय-प्रमाणपत्र बताता है कि कभी वे एक महीने में 50,000 रुपए कमाते थे. अब वे सिर्फ़ 10,000 रुपए के आसपास ही कमा पाते हैं. पैसों की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रिश्तेदारों से क़र्ज़ लेना पड़ता है. रिश्तेदार जितने क़रीबी होते हैं ब्याज की दर उतनी कम होती है. बाद में तैयार मालों की बिक्री के बाद वे अपना क़र्ज़ चुकाते हैं, लेकिन महामारी के बाद से उनकी बिक्री बहुत कम हुई है.
“कोविड हमारे लिए अच्छा समय था,” तनु बताती है. “ बाज़ार बिल्कुल शांत था. हमारे लिए राशन का अनाज लेकर सरकारी ट्रक आते थे. मास्क बांटने के उद्देश्य से दूसरे लोग भी आते थे.”
सलमा को अधिक शिकायतें हैं, “महामारी के बाद लोग हमें संशय की नज़र से देखने लगे हैं. उनकी आंखों में हमारे प्रति एक घृणा दिखती है.” जब कभी वे बाहर निकलते हैं, तो स्थानीय लोग उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्हें जातिसूचक गलियां देते हैं.
“वे हमें अपने गांव में नहीं रहने देते हैं. मेरी समझ में नहीं आता कि वे हमारी जात को गालियां क्यों देते हैं.” सलमा चाहती हैं कि दुनिया उन्हें भी बराबरी का दर्जा दे. “रोटी तो रोटी होती है - हमारे लिए और उनके लिए भी. सब एक ही चीज़ तो खाते हैं. हमारे और उन अमीरों के बीच क्या अंतर है?”
अनुवाद: प्रभात मिलिंद